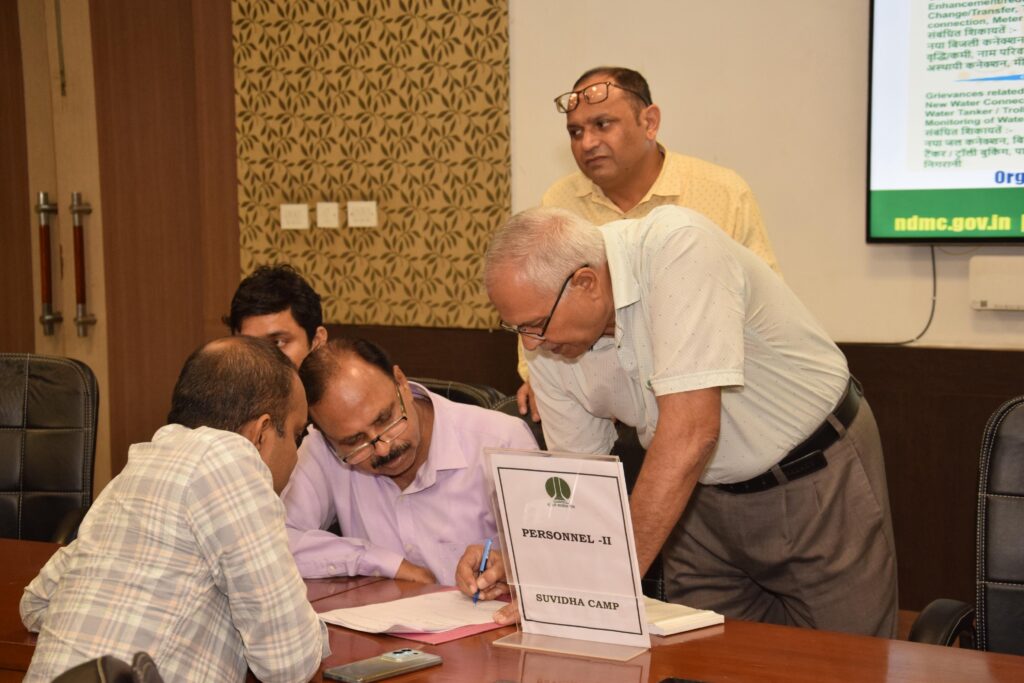“खेल प्रशिक्षण”
भूमिका _दरअसल खेलकूद में प्रशिक्षण की आवश्यकता बहुत समय से स्वीकार की जाती रही है, समाज में खेलों का दर्जा बढ़ने से खेलकूद प्रशिक्षण और भी महत्वपूर्ण हो गया है। प्रशिक्षण एक व्यक्ति को किसी गतिविधि या काम के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं ।खेलकूद में हम प्राय: यह खेलकूद प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ है खिलाड़ियों को उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना। परंतु आजकल खेलकूद प्रशिक्षण केवल एक शब्द ही नहीं है बल्कि अब यह एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है जो प्रत्येक उस व्यक्ति को प्रभावित करता है जो शारीरिक व्यायाम की गतिविधियों या खेलकूद स्वास्थ्य, स्फूर्ति अथवा विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए अपनाते हैं। अतः हमारी आज की चर्चा का केंद्रबिंदु खेल प्रशिक्षण है।
यह सत्य है कि दूसरे कारकों के अलावा, किसी व्यक्ति का किसी खेल में प्रदर्शन उसकी शारीरिक, संरचनात्मक व मनोवैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करता है। लोग शारीरिक क्षमताओं, मानसिक क्षमताओं तथा संरचनात्मक क्षमताओं मनोवैज्ञानिक योग्यताओं तथा व्यक्तित्व के गुणों में अलग-अलग होते हैं।लोग न केवल दूसरों से ही भिन्न होते हैं अपितु वे स्वयं में भी एक योग्यता व दूसरी योग्यता में भिन्न-भिन्न होते हैं। व्यायाम शारीरिक संरचना विशेषज्ञ, खेल वैज्ञानिक ,शारीरिक शिक्षा प्रदान करने वाले व खेल प्रशिक्षण विशेषज्ञ कई ढंग तथा तरीके सुझाते हैं जिनसे इन मानवीय योग्यताओं व क्षमताओं में वृद्धि की जा सके ।विभिन्न प्रयोगों के आधार पर व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि करने के नए ढंग सुझाए गए हैं ।कहा जाता है कि मनुष्य की क्षमताएं असीमित होती हैं तथा यह तब सच लगता है जब हम विश्व स्तर के खिलाड़ी व एथलीटों का अभूतपूर्व प्रदर्शन देखते हैं ।ऐसे प्रदर्शन का आधार व्यक्ति की सोच तथा खेल प्रशिक्षण होता है। जिससे खिलाड़ी शारीरिक रूप से फिट बनता है और वह प्रतियोगिता में अभूतपूर्व प्रदर्शन कर अपना और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करता है।
हरदयाल सिंह के अनुसार ” खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है”।
इसी प्रकार मैटविज्यू के
शब्दों में “खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी के आधार स्वरूप है”।
इस आधार पर हम खेल प्रशिक्षण के उद्देश्य मोटे तौर पर देख लेते हैं जो निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं-व्यक्तित्व का विकास । शारीरिक तंदुरुस्ती का विकास। हुनर तकनीक का विकास।
कौशल का विकास व मानसिक प्रशिक्षण।
अर्थात ‘प्रतियोगी खेलों में खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिस्पर्धाओं में खिलाड़ियों को उच्चतम संभव खेल प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार करना है’।
अब हमारे लिए यह जानना भी जरूरी है कि वह कौन से सिद्धांत है जिन्हें अपना कर,खेल प्रशिक्षण के लक्ष्य व उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है-अतः वे सिद्धांत निम्नलिखित प्रकार से हैं-
अतिभार का सिद्धांत। व्यक्तिगत विशेषता का सिद्धांत।प्रगतिशील विकास का सिद्धांत।विशेषज्ञता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत।सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत। अवधिकालीनता का सिद्धांत आदि।
उपर्युक्त सिद्धांतों के अंतर्गत खेल प्रशिक्षण के विभिन्न कारक का उपयोग किया जाता है,
जैसे-पहला-शक्ति( स्ट्रैंथ)शक्ति के भी तीन प्रकार हैं, अधिकतम शक्ति। विस्फोटक शक्ति। व
शक्ति सहनशीलता।
दूसरा- चाल (स्पीड), चाल योग्यता के भी पांच प्रकार हैं_ प्रतिक्रिया योग्यता ।गति की चाल। त्वरण योग्यता। प्रचलन योग्यता।व चाल सहनशीलता।
तीसरा_सहनशीलता (एंडोरेंस)इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार आते हैं-
जैसे मूलभूत सहनशीलता है। सामान्य सहनशीलता,विशिष्ट सहनशीलता।सूक्ष्म सहनशीलता। मध्यकालीन सहनशीलता व
दीर्घकालीन सहनशीलता है।
चौथा- लचीलापन,इसके दो प्रकार हैं-क्रियाशील लचीलापन व अक्रियाशील लचीलापन।
पांचवा_समन्वय योग्यता(कोऑर्डिनेशन), इसके सात प्रकार हैं-पृथक्करण की योग्यता। निर्धारण योग्यता। युग्मन योग्यता।प्रतिक्रिया योग्यता। संतुलन योग्यता। तालमेल योग्यता व अनुकूलन योग्यता।
संक्षेप में-
हम कह सकते हैं कि खेल प्रशिक्षण किसी कार्य( फिजिकल फिटनेस )को करने के लिए तैयारी की प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसके माध्यम से एक खिलाड़ी को इस स्तर पर तैयार किया जाता है कि वह खेल प्रतिस्पर्धाओं में उच्च स्तर का प्रदर्शन कर सके।