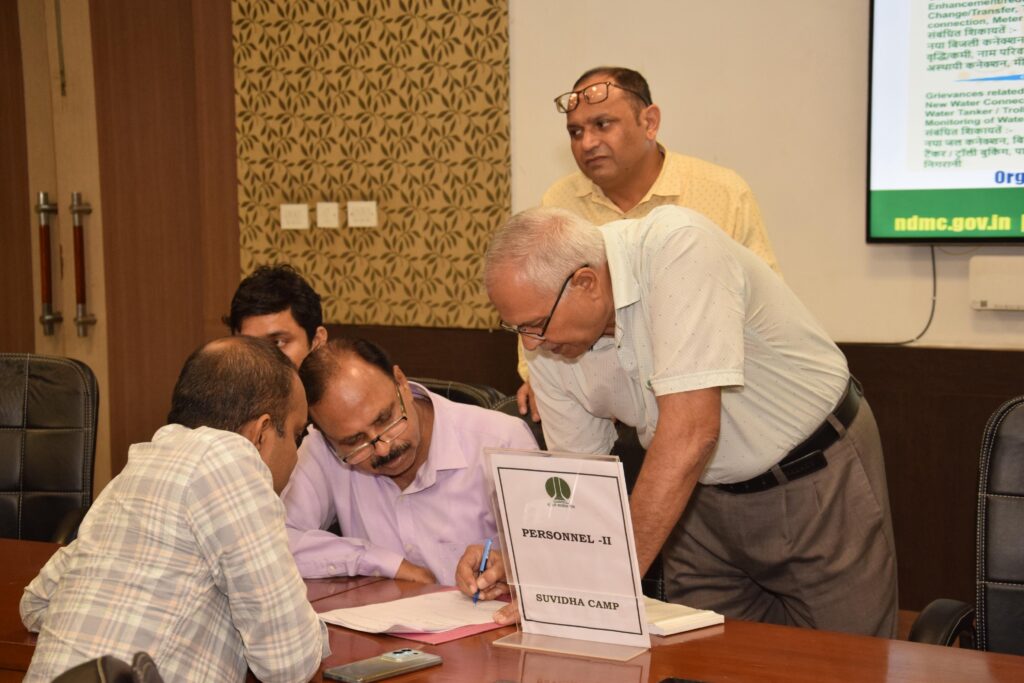“रुचि”
भूमिका_ रुचि या शौक़ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आनंद के लिए अवकाश (फुर्सत )के समय की
जाए। इनमें खेल ,मनोरंजन, कला, संगीत, किसी विषय का अध्ययन या उससे संबंधित चीजें इकठ्ठी करना इत्यादि शामिल हैं। अतः हमारी आज की चर्चा इसी परिप्रेक्ष्य में होने वाली है-
जीवन बहुत नीरस तथा रंगीन हो जाए अगर व्यक्ति के पास करने के लिए कोई काम न हो।जिस व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत रुचि अथवा ध्येय नहीं होता बोरियत तथा कुंठा उसके प्राय: मित्र बन जाते हैं। रुचि जीवन में दिशा का बोध तथा स्थायित्वत लाते हैं। ये हमारे रोजमर्रा के कामों को उत्प्रेरणा देते हैं तथा उन्हें रुचिकर बनाते हैं तथा मुश्किलों में हमें आगे बढ़ाने में मदद देते हैं। रुचि कोई गतिविधि नहीं है। यह एक स्थाई रुझान तथा मानसिक ढांचा है जो स्नायु गतिविधि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रेरणात्मक ऊर्जा देता है । रुचि किसी गतिविधि का कारण हो सकती है तथा उस गतिविधि में भाग लेने का परिणाम हो सकता है। रुचि उस प्रेरणात्मक बल का नाम है जो हमें आगे बढ़ाता है कि हम व्यक्ति ,चीज या गतिविधि को ध्यान देते हैं या गतिविधि द्वारा उत्प्रेरित या प्रभावी अनुभव भी हो सकता है।
ड्रिवर ने रुचि की परिभाषा यूं दी है,”किसी गतिशील पहलू में रुचि एक प्रकट गुण है।”
रुचि तब विकसित होती है जब हमें भूतकाल में कोई संतुष्टि मिली हो या भविष्य में संतुष्टि मिलने वाली हो।
यहां बहुत महत्वपूर्ण बात यह है की असफलता के बाद की आशा में भी लगातार रुचि छुपी होती है।
अपने गुणों, ध्यान ,सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रतिष्ठा के अनुसार अलग-अलग व्यक्तियों की अलग-अलग रुचिया होती हैं।
जो रुचियां हम अपनाते हैं वह ज्यादातर हमारे अनुभव पर आधारित होती है।
एक बच्चें की रुचियां है उसके व्यक्तित्व की बनावट दर्शाती है।
विशेष कर अपने बारे में उसके विचारों पर किस तरह पूर्व के अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। जबकि बच्चे ग्रुप गतिविधियों में अपनी रुचियां विकसित करते हैं, इसके साथ-साथ भी सामाजिक व तकनीकी हुनरों का विकास भी करते हैं।अपनी रुचियों
की तलाश में रचनात्मक अभिव्यक्ति तथा सामाजिक मेलजोल के लिए अवसर भी पा लेते हैं। रुचियों से कई नए क्षेत्रों में खोजपूर्ण गतिविधियों की जाती हैं।
व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा क्लासरूम योजना में जब रुचियों का प्रयोग करते हैं तो ऐसी समझ बहुत मदद करती है।
जैसी रुचि व्यक्ति विकसित करता है उससे उसकी पसंद तथा नापसंद का पता चलता है। इस पसंद और ना पसंद का दायरा व्यक्ति की योग्यताओं तथा वातावरण में अवसरों द्वारा परिवर्तित होता रहता है।
अगर उसका मानसिक स्तर काफी ऊंचा है तो व्यक्ति गति- विधियों में सफलतापूर्वक स्वयं को लगा सकता है।
इस तरह व्यक्ति का वातावरण अगर समृद्ध है तो उसे अपने अनुभव व्यापक करने के बहुत से अवसर मिलते रहते हैं।
उसके कार्यों के चुनाव की दिशा क्या होगी यह उसकी जरूरतों तथा मूल्य व्यवस्था पर निर्भर है।
केवल वही गतिविधियां उसे आकर्षित करेंगे जो उसकी संबंध मांगों को पूरा करती है।
यदि ज़रूरतें संभावनाओं के कम दायरों में संतुष्ट होती हैं तो उसके अनुरूप रुचियां भी सीमित हो जाएगी।
अर्थात आवश्यक नहीं की हर समय रूचियां एक समान रहें।
जिन कार्यों या वस्तुओं से हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती उनमें हमारी रुचि ज्यादा देर तक नहीं रहती।
जब कार्य सिद्ध हो जाए अथवा जरूरत पूरी हो जाए उस कार्य व वस्तु में व्यक्ति की रुचि खत्म हो जाती है।
इसके विपरीत जब कार्य या वस्तु से हमारी स्थाई जरूर जुड़ी हुई है तो उसमें हमारी रुचि स्थाई होगी तथा जरूरत पूरा करने के लिए वह कार्य हमें रूचिकर लगता रहेगा।
रुचिया व्यक्तित्व के स्थाई गुणों से कुछ अधिक होती हैं तथा गत- विधियों के समूह से बढ़कर होती हैं।
रुचियों में महत्वपूर्ण गतिशील गुण होते हैं।
रुचिया ज्यादातर बचपन से बन जाती है परंतु उन्हें बाद में भी अपनाया जा सकता है।
संक्षेप में-
हम कह सकते हैं कि रुचियों के विकसित होने के कारण तथा उन रुचियों को पूरा करने से संबंधित गतिविधियों से व्यक्ति के हुनर और योग्यताओं की परीक्षा होती है।इस प्रक्रिया में वह अपने व्यक्तिगत गुणों ,योग्यताओं, क्षमताओं, ताकत व कमजोरीयों का सही ज्ञान प्राप्त करता है।
इस माध्यम द्वारा वह सामाजिक वातावरण के गुणों के बारे में सीखता है तथा यह जान लेता है, भौतिक वातावरण में कैसे स्रोत उपलब्ध हैं तथा कौन से माध्यम या हुनर हैं जिनके द्वारा वह उस उच्च सीमा तक व्यक्तिगत रूप से कैसे पहुंच सकता है जहां जीवन पूर्णता को प्राप्त होता है।